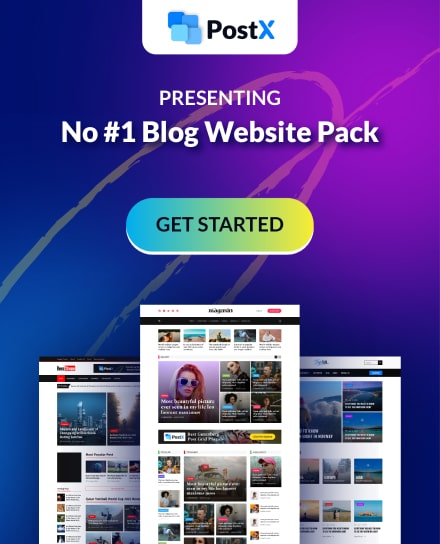यह कोई भावुक कहानी नहीं, बल्कि बिहार के विकास के दावों पर खड़ा एक कड़वा सवाल है। सहरसा ज़िले के नवहट्टा अंचल का यह महादलित टोला आज भी उस भारत की तस्वीर दिखाता है, जहाँ आज़ादी के दशकों बाद भी इंसान को न जीने की ज़मीन मिली है, न मरने की।
यहाँ घर का आंगन ही श्मशान बन चुका है।
यहीं जन्म होता है, यहीं ज़िंदगी पलती है और यहीं मौत को मिट्टी में दफ़्न कर दिया जाता है।
टोले में कदम रखते ही सरकारी योजनाओं की असलियत बेनक़ाब हो जाती है। कच्ची झोपड़ियाँ, फूस की छतें, मिट्टी की दीवारें और उन्हीं आंगनों में बनी क़ब्रें। यह दृश्य किसी आपदा क्षेत्र का नहीं, बल्कि उस राज्य का है जो “सामाजिक न्याय” को अपनी पहचान बताता है।
महादलित परिवारों को आज तक न पाँच डिसमिल ज़मीन मिली, न आवास योजना का लाभ। नतीजा यह है कि जब किसी की मौत होती है, तो दाह-संस्कार का सवाल ही पैदा नहीं होता। मजबूरी में शव को अपने ही आंगन में दफ़्न कर दिया जाता है।
सुनील सादा, जिनकी आँखों में वर्षों की बेबसी झलकती है, कहते हैं—
“साहब, ज़मीन नहीं है तो श्मशान कहाँ ले जाएँ? मरने के बाद भी ग़रीब को जगह नहीं मिलती।”
उनकी आवाज़ काँप जाती है। यह सिर्फ़ एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि सैकड़ों महादलित परिवारों की साझा चीख़ है।
सरकार के काग़ज़ों में तीन डिसमिल ज़मीन का आवंटन दर्ज है, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि वह ज़मीन आज तक किसी ने देखी ही नहीं। नवहट्टा अंचल कार्यालय से लेकर सहरसा ज़िला मुख्यालय तक अर्ज़ियाँ दी गईं, फ़ाइलें चलीं, दस्तख़त हुए—मगर इंसाफ़ नहीं पहुँचा।
यह टोला अब सवाल पूछ रहा है—
क्या ग़रीब की मौत की कोई क़ीमत नहीं?
क्या महादलित होना इतना बड़ा अपराध है कि जीते-जी ज़मीन न मिले और मरने के बाद भी?
हर आंगन यहाँ एक सवाल है और हर क़ब्र सरकार के लिए एक इल्ज़ाम। यह सिर्फ़ ज़मीन की लड़ाई नहीं, यह वजूद, इज़्ज़त और इंसानियत की जंग है—जो आज भी बिहार के एक महादलित टोले में दबी पड़ी है।
अगर अब भी सरकार नहीं जागी, तो यह सिर्फ़ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की खुली कब्र मानी जाएगी।
पटना से राहुल कुमार की रिपोर्ट